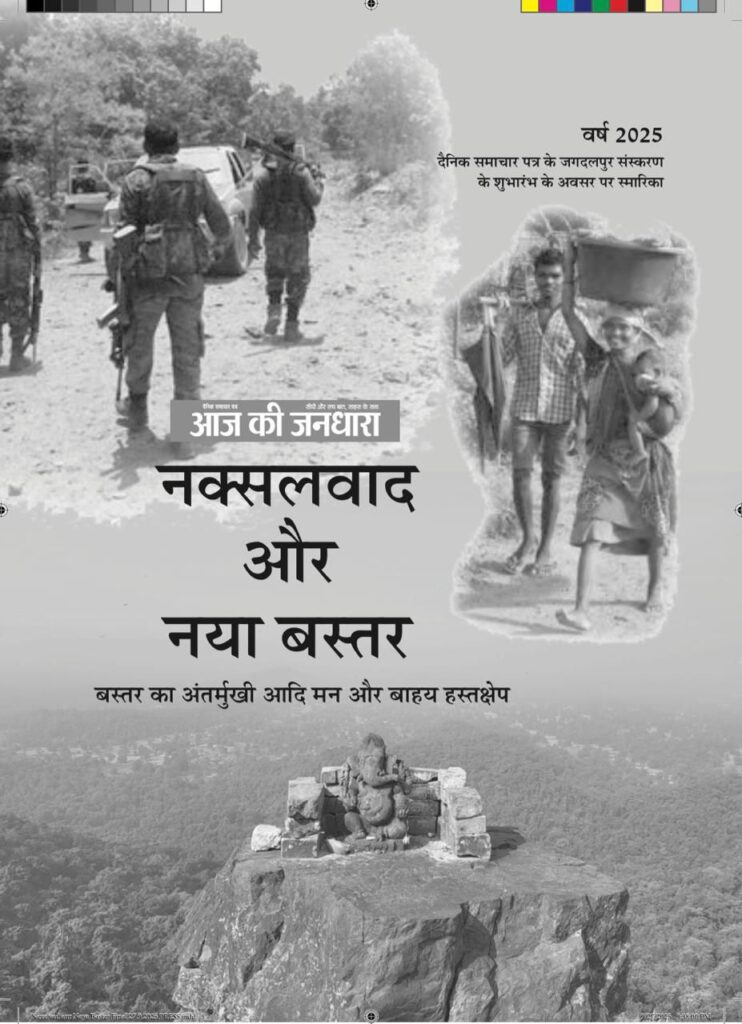गांधीवादी विचारक कनक तिवारी वरिष्ठ लेखक, पूर्व महाधिवक्ता और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अध्ययनशील, मुखर और तर्कसंगत वक्ता के रूप में वे जाने जाते हैं। हमने उनसे नक्सलवाद, नया बस्तर, अंतर्मुखी आदिम-मन और बाह्य हस्तक्षेप पर लिखने का आग्रह किया था। उनका यह लेख हमारी स्मारिका और आज की जनधारा में प्रकाशित किया गया है, जिसे अब सोशल मीडिया पर भी साझा किया जा रहा है। कृपया इसे पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें।
⸻
(1)
9 अगस्त को दुनिया ने तय किया कि उसे विश्व आदिवासी दिवस (World Indigenous Peoples’ Day) मनाना चाहिए। इस शब्द को लेकर कई पेच हैं। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपने सदस्य देशों के साथ 1957 में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे Indigenous and Tribal Populations Convention (No. 107) कहा गया। यह सम्मेलन दुनिया के सभी नस्लों और प्रकृति के आदिवासियों के जीवन से जुड़े सवालों को सुलझाने की दिशा में एक अच्छी पहल थी।
1989 के कन्वेंशन में इसमें आंशिक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। दरअसल 1985 तक ही यह तय हो गया था कि अलग-अलग देशों के आदिवासी समुदायों को किसी एक ढांचागत परिभाषा के तहत नहीं बाँधा जा सकता। इसलिए परिभाषा को लचीला बनाए जाने की जरूरत थी। मूल आदिवासियों के साथ उन समूहों को भी जोड़ा गया जो बाद में विभिन्न देशों में बस गए। 1989 के इस कन्वेंशन पर कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिनमें भारत भी शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए आज यह संशय उठाया जाता है कि आदिवासी कौन हैं, जबकि स्वयं आदिवासियों को अपने अस्तित्व पर कोई संशय नहीं है।
⸻
(2)
आदिवासियों का धर्म क्या है — इसका सर्वसम्मत उत्तर आज भी नहीं मिल सका है। परिस्थितियों में जानबूझकर उलझनें पैदा की जाती रही हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रश्न कब हल होगा। अंग्रेजी हुकूमत के समय भारत में 1891 की जनगणना में आदिवासियों के लिए कॉलम था — Forest Tribe।
1901 में इसे Animist (प्रकृतिवादी) लिखा गया।
1911 में Tribal Animist,
1921 में Hill and Forest Tribe,
1931 में Primitive Tribe,
और 1941 में केवल Tribes लिखा गया।
आजादी के बाद 1951 की मर्दुमशुमारी में आदिवासी आबादी को दर्शाने वाला कॉलम ही हटा दिया गया। यही कारण है कि आज भी भारत के आदिवासी अपनी पहचान को लेकर संशय और असुविधा में हैं।
⸻
(3)
भारत की संविधान सभा दिसंबर 1946 में गठित हुई और 20 नवंबर 1949 तक चली। संविधान सभा के मूल उद्देश्यों पर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर की असाधारण भूमिका रही, लेकिन समानांतर रूप से कुछ अन्य सदस्यों की भूमिका भी उल्लेखनीय थी, जिन्हें इतिहास में उपेक्षित किया गया — जैसे प्रोफेसर के. टी. शाह, जिन्होंने कई बार अंबेडकर के समानांतर तर्कपूर्ण बहसें कीं।
इसी प्रकार, संविधान सभा में आदिवासी प्रश्नों पर सबसे मुखर और तार्किक बहस तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) से निर्वाचित सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। दुर्भाग्य से न तो उन्हें आदिवासी समाज ने ठीक से पढ़ा-समझा, न प्रचारित किया। मेरा मानना है कि संविधान निर्माण में आदिवासियों के साथ अन्यायपूर्ण अनदेखी की गई। यह नाइंसाफी न भोलेपन से हुई, न ही उसकी माफी दी जा सकती है।
⸻
(4)
महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्हें आदिवासी समस्याओं पर उतना ध्यान देने का अवसर नहीं मिल सका, जितना मिलना चाहिए था। इसलिए उन्होंने अपने 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम में ‘आदि सेवा’ को शामिल किया। गांधीजी के शिष्य अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें इतिहास ने ठक्कर बापा के नाम से प्रसिद्ध किया, जीवनपर्यंत मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले और गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच कार्यरत रहे।
संविधान सभा के लगभग 275 सदस्यों में से केवल पाँच आदिवासी सदस्य थे। इस पर जयपाल सिंह मुंडा ने 11 दिसंबर 1946 को कहा था कि “हम करोड़ों की संख्या में हैं, परंतु हमारी आवाज़ केवल पाँच प्रतिनिधियों तक सीमित कर दी गई है।”
यह भी विडंबना थी कि संविधान सभा की आदिवासी उपसमिति के अध्यक्ष ठक्कर बापा बनाए गए, किसी आदिवासी को नहीं। मुंडा ने इस पर आपत्ति जताई कि इस तथाकथित सलाहकार समिति में कम से कम एक आदिवासी सदस्य तो होना ही चाहिए। अल्पसंख्यकों के नाम पर सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और पारसियों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिला, पर आदिवासियों को नहीं। ठक्कर बापा को गांधी और संविधान सभा में अनुपातहीन महत्व दिया गया। वे कई बार यह कहकर अहंकार जताते थे कि “जयपाल सिंह मुंडा से अधिक मुझे आदिवासी इलाकों और समस्याओं की जानकारी है।”
⸻
(5)
सरदार पटेल ने नृविज्ञानिक दृष्टि से यह घातक टिप्पणी की थी कि “हम चाहते हैं कि आदिवासियों का जीवनस्तर इतना ऊँचा उठाया जाए कि वे हमारे स्तर तक पहुँच जाएँ,” और उन्होंने संविधान से ‘Tribe’ शब्द हटाने की बात कही। यह अत्यंत खतरनाक विचार था। इस पर जयपाल सिंह मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा कि “मुझे खेद है कि सरदार पटेल ने मेरे विचारों का गलत अर्थ निकाला है।”
आज बस्तर में अमित शाह जो कर रहे हैं, वह उसी सोच की पुनरावृत्ति है — न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। नक्सलवाद तो केवल मुखौटा है।
⸻
(6)
संविधान सभा में आदिवासी नेताओं को सबसे अधिक भरोसा जवाहरलाल नेहरू पर था। उन्होंने कई बार कहा कि “जो नेहरू कहेंगे, हम वही मानेंगे।” लेकिन इतिहास ने नेहरू को आदिवासी समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
1959-60 में रायपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के दबंग आदिवासी नेता लाल श्याम शाह के नेतृत्व में लाखों आदिवासी एकत्र हुए और नेहरू को अपने बीच बुलाने का आग्रह किया। नेहरू ने सभा को संबोधित कर कई आश्वासन दिए। इनका ब्यौरा हमारे सहयोगी लेखक सुदीप ठाकुर की पुस्तक लाल श्याम शाह की कहानी में विस्तृत रूप में मिलता है।
नेहरू ने आदिवासियों के लिए ‘पंचशील’ के रूप में पाँच बुनियादी सिद्धांत दिए:
1. आदिवासी अपनी चेतना और बोध के अनुसार आगे बढ़ें।
2. जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार माना जाए।
3. वे अपने कार्यक्रम स्वयं तैयार करें।
4. उनके इलाकों में प्रशासनिक हस्तक्षेप और योजनाओं की भरमार न हो।
5. विकास को आँकड़ों से नहीं, मानवीय गुणवत्ता से आँका जाए।
परंतु इन सिद्धांतों पर कभी अमल नहीं हुआ।
⸻
(7)
जयपाल सिंह मुंडा का स्पष्ट मत था कि भारत के वास्तविक मूल निवासी केवल आदिवासी हैं। नेहरू ने अपनी पुस्तक Discovery of India में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई आदिवासी गणराज्य विद्यमान थे। मुंडा को इस बात पर कड़ा ऐतराज था कि बिना विचार किए ‘आदिवासी’ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जनजाति’ शब्द प्रयोग में लाया गया। यद्यपि डॉ. अंबेडकर ने इसकी सफाई दी, पर मुंडा उससे संतुष्ट नहीं हुए।
⸻
(8)
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि आदिवासियों की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित पाँचवीं अनुसूची को 19 अगस्त 1949 को स्वीकृत करने के बाद, 5 सितंबर 1949 को डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में संशोधित कर दिया गया। पहले प्रावधान था कि राज्यपाल आदिवासी सलाहकार परिषद की सलाह के अनुसार विधायी कार्य करेंगे, जिसे बदलकर सिर्फ सलाह लेंगे कर दिया गया। यहीं से आदिवासी अधिकारों की हत्या शुरू हुई।
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और वह राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करता है। हालांकि पाँचवीं अनुसूची में राज्य सरकार की सलाह आवश्यक नहीं है, फिर भी व्यवहार में वही हावी रहती है।
⸻
(9)
संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रारंभ में यह था कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ‘consultation’ शब्द का अर्थ सहमति कर दिया। प्रश्न यह है कि यही अर्थ राज्यपाल और आदिवासी मंत्रणा परिषद के संदर्भ में क्यों नहीं लागू किया जाता?
आदिवासियों को आज भी हिन्दू और ईसाई धर्मों के झूले में झुलाया जा रहा है। नेहरू ने 1955 में हिन्दू कोड बिल बनाया, जो आदिवासियों पर लागू नहीं हुआ, फिर भी उन्हें हिन्दू कोड बिल की परिधि में रखा गया — यह विरोधाभास आज भी कायम है।
⸻
(10)
अंततः यह जानना आवश्यक है कि संविधान ने आदिवासियों के लिए वास्तव में किया क्या है। संविधान एक सामूहिक और प्रामाणिक दस्तावेज है — और यह सुखद है कि यह दुनिया का पहला असांप्रदायिक, समावेशी ग्रंथ है, जो बाइबिल, कुरान, वेद, गीता या गुरु ग्रंथ साहिब से अलग अपनी प्रकृति में मानवीय है। इसे तीन सौ से कुछ कम सदस्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से लिखा — लेकिन उसमें भी आदिवासियों की पीड़ा और न्याय की पुकार अधूरी रह गई।