उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंदजी के नाम से भला कौन परिचित नही है. उन्होने अपनी लेखनी के माध्यम से देश प्रेम और सामजिक समरसता की यर्थाथ रचना की.मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है. उनकी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ फिल्म आर्ट एंड विजुअल सोसायटी और रायपुर के रंग संस्थाओं के सहयोग से 5 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन सड्डू स्थित जनमंच में किया जा रहा है. रविवार को जानेमाने कथाकार आलोचक भालचंद्र जोशी भी पहुंचे और उन्होने व्याख्यान के माध्यम से मुंशी प्रेम चंद जी के लेखन शैली पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनकी विशेषताएं बताई.

व्याख्यान की शुरूआत करते हुए भालचंद्र जोशी जी ने कहा कि प्रेमचंद जी मेरे ही नही अपितु सभी लेखकों के पुरखे हैं हमारे पितामह की तरह है. कहानी या उपन्यास की बात हो हर बात उन्ही से शुरू होती है. कहानी या उपन्यास की बात उनके बिना अधूरी है. 1907 में उन्होने पहली कहानी एक अनमोल रतन लिखी थी. 1918 में उनका पहला उपन्यास आया था सेवा सदन. कहानी की लंबी परंपरा उन्होने शुरू की थी 1936 तक कफन जैसी चर्चित कहानियां लिखी. अपने अंतिम दिनों में प्रेमचंद जी ने कई कालजयी रचनाएं लिखी. कहानी के रूप् में कफन और उपन्यास के रूप में गोदान. उन्होने नाटक भी लिखे जिसमें करबला 1923, संग्राम 1924 और 1933 में प्रेम की वेदी लिखी. उन्होने केवल 3 ही नाटक लिखे लेकिन कहानी और उपन्यास की लंबी श्रृंखला है.
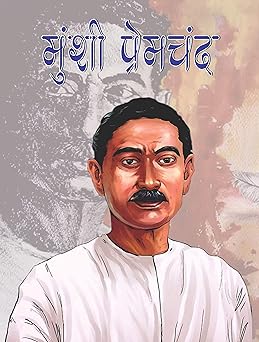
वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे लेकिन इसकी रचना अधूरी छोड़ वे दुनिया को अलविदा कह गए. उनकी इस रचना को उनके बेटे अमृतराय ने पूरा किया वे भी एक अच्छे लेखक थे 1948 में वह उपन्यास प्रकाशित हुआ. उसके बाद उनकी कई रचनाओं को पुन: प्रकाशित किया गया. उनका अपना प्रेस था जिसका नाम सरस्वती प्रेस था. जहां से कई पत्रिकांए प्रकाशित होती थी. इनमे से सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी हंस जो कि साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही खास है. इस पत्रिका के बिना साहित्य और हिंदी पत्रकारिता दोनों अधूरे हैं
भालचंद्र जोशी ने कहा कि एक लेखक कैसे जिता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रेम चंद जी है. विश्व के कई प्रख्यात लेखक मोपासा, चेखव और टालस्टाय के बारे में जानते है कि वे हमेशा साहित्य को ही जीते आए है लेकिन प्रेमचंद जी इनसे भी बढ़कर थे. वे सारे समय ही साहित्य की ही बाते करते थे. प्रेमचंद जी जब बहुत बीमार थे तब भी वे साहित्य की बात करते थे उनसे मिलने जैनेंद्र जी आए थे तो वे उनसे केवल साहित्य की ही बात करते रहे. वे उस समय के वर्तमान दौर के लेखकों के बारे में बात कर रहे थे.

भालचंद्र जोशी
भालेंद्र जोशी ने कहा कि मुंशी प्रेम चंद पर कई तरह के आरोप भी लगे उन पर ब्राम्हण विरोधी होने का आरोप लगा तो किसी ने उन्हे ब्राम्हणवादी बताया, कुछ ने कहा कि वे स्त्री विरोधी लेखक हैं. लेकिन इसको समझने के लिए किसी संदर्भ को देखना चाहिए जैसे एक ब्रिटिष लेखिका शार्लोट ब्रोंटे हैं. उनहोने दो तरह के उपन्यास लिख लेखक जो होता है चरित्र को लिखता है. उस समय को लिखता है चरित्र को लिखता है. और उस समय के जरूरत को लिखता है. उन्होने जेन आयर उपन्यास लिखा जो स्त्री पक्षधरता की बातें है. लेकिन उन्होने ही द ओल्ड मिस्ट्रेस जैसा उपन्यास लिखा जिसमें स्त्री खलनायिका के रूप् में थी. इसी तरह शरतच्रदं ने स्त्री चरित्र को मार्मिकता से उतारा था ठीक वैसे ही शरतचंद जी ने मंझली दीदी में कादंबिनी जैसा चरित्र लिखा जो उस समय की जरूरत थी. ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखा उन्होने घिसू-माधव चरित्र लिखा तो कहा गया कि दलितों को नीचा दिखाने लिखा. लेकिन उन्होने कफन को लिखा तो उस कालखंड को लिखा वे बता रहे थे कि लोग शराब पीने के लिए कफन तक को बेच देते थे. वे दलित को नही बता रहे थे वे बता रहे थे कि उस समय लोग कैसे बदल रहे थे. ठीक ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में कहा गया था. उन्होने शुद्र के खिलाफ लिखा तो शबरी के लिए भी मार्मिक वर्णन किया. लिखते हुए लेखक के मन में कभी ऐसी बात नही आती. हां ये जरूर है कि वे उन्हे अपने समय की आहट और संकेत आ जाती है. जब जिस तरह के चरित्र की जरूरत होती है वे उसी तरह की रचना किया था. इसी तरह ठाकुर का कुंआ की रचना वैसी थी. उनके लिए ब्राम्हण, शुद्र, ठाकुर सभी एक समान थे. वे उस समय सामाज की अमानवीयता को बताया. समाज के यर्थाथ को उन्होने दिखाया अपने चरित्र के माध्यम से लिखा.
आदर्शोन्मुखी यर्थाथवाद पर उन्होने लिखा उन्होने अपने समय के दौरान की स्थिति को देखकर ही रचना की. आजादी के समय तो सारा जोर आजादी लेने के लिए था. उन्होने सभी को स्वार्थ तोड़ आगे आने के लिए प्रेरित किया. ताकि सभी मानवीयता और परोपकार बना रहेगा. इसलिए उन्होने वैसी ही रचना की. जिस तरह गांधी जी ने रामराज की कल्पना की वैसे ही प्रेमचंद जी ने की थी. कबीर दास जी ने कई सारी चीजें नाथपंत से लिया. लेकिन शून्यवाद उनका अपना था. गांधी जी ने भी अहिंसा बुद्ध और महावीर स्वामी से ली. लेकिन सत्य उनकी अपनी खोज थी. ऐसी ही आदर्शोन्मुखी यर्थाथवाद मुंशी प्रेमचंद की अपनी खोज थी. इसलिए वे बड़े कहानीकार और उपन्यासकार थे. जब तक कोई लेखक स्वयं का नही देगा तब वह लोगों से नही जुड़ पाएगा. गांधी जी ने कहा राजनीतिक आजादी मिल जाए और बात है लेकिन आर्थिक आजादी मिलना सबसे बड़ी बात है. हर आदमी को काम मिले हर आदमी समाज में बराबर हो. गांधी जी ने आजादी मिलने के बाद यह बात कही जबकि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में ही कह दिया था. उन्होने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज न बैठ जाए.

आज के दौर में कोई ऐसा लेखक नही है जिसने 300 रचनांए लिखी. वे भी हर विषय पर. इसी में एक शतरंज के खिलाड़ी है. जिसमें दो नवाबों के माध्यम से नवाबी चरित्र का वर्णन किया. बताया गया कि कैसे महल में आक्रमण को हो गया. सत्ता उनके हाथ से जा रही है. पर नवाबों को कोई चिंता नही थी. इसी तरह बड़े भाई साहब मार्मिक कहानी है. कि छोटा भाई सफल हो रहा है. भाई को महसूस होता है कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है. दो बैलों की आत्मकथा इतनी मार्मिक है कि जानवरों के बारे में भी कोई ऐसा लिख सकता था वे उस समय की जानवरों को लेकर लिखी गई पहली कहानी थी.
इसी तरह नमक का दरोगा ऐसा कहानी है जो उस दौर के कालखंड का वर्णन कर देती है. रचना में यह दिखाया गया कि कैसे आजादी के दौर में आम आदमी को सामान्य सी चीज उपलब्ध नही थी. वे आदर्श और चरित्र की बात अपनी कहानी के माध्यम से दर्शाते थे. मानवीयता के साथ किया गया काम ही मनुष्य को इतिहास में जीवित रखता है. ऐसा ही मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने समय को जिस दृष्टि से देखा वह वृहत थी. उनकी इसी दृष्टि ने उन्हें महान लेखक बनाया. गांधी जी में सांस्कृतिक आत्म विश्वास बहुत बड़ा था तो प्रेमचंद में सामाजिक आत्म विश्वास था. गांधी जब सांस्कृतिक भूमिका को देख रहे थे तो प्रेमचंद जी समाज में बदलाव के लिए लेखन की भूमिका को देख रहे थे. वे मानते थे कि साहित्य से क्रांति नही होती लेकिन बदलाव की भूमिका साहित्य ही तय करता है.
भालचंद्र जोशी ने बताया कि जब नेहरू जी झंडावंदन के लिए जा रहे थे तब वे सीढ़ी चढ़ते हुए लड़खड़ा गए तब रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संभाला. तो नेहरू जी ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने मुझे संभाल लिया वरना मैं गिर जाता. तो दिनकर जी ने जवाब दिया कि साहित्य का काम हमेशा दूसरों को संभालना होता है. हम गिरते हुए लोगों को संभाल लेते हैं.
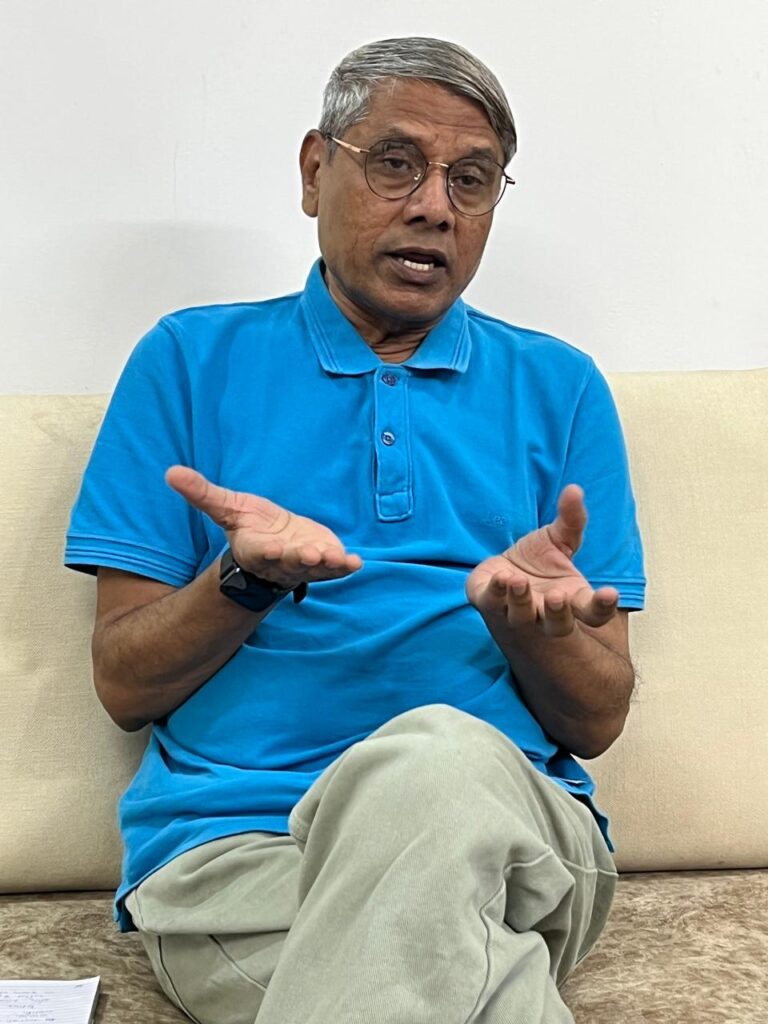
मुंशी प्रेमचंद जी को लेकर कहा गया कि उनमें प्रेम नही था. पर सवा सेर गेंहू उनकी ऐसी रचना है कि उसमें पति-पत्नी का आगाध प्रेम नजर आया दृउसमें संवेदना और मार्मिकता थी. उन्होंने प्रेम और संवेदना को सुंदर तरिके से वर्णन किया है. प्रेमचंद जी ने भले ही प्रेमिका के प्रेम का वर्णन नही किया लेकिन पति-पत्नी के प्रेम को अपने पात्रों में शानदार तरिके से उतारा. उन्होने अपने पात्रों में यार्थाथ को लिखा उन्होने दिखाया कि समाज कैसे बदल रहा है चालाक हो रहा है. देश प्रेम से लेखनी की शुरूआत की थी वो समय के साथ यर्थावाद की ओर चला गया वे चीजों को गहराई में जाकर देखते थे.
भालचंद्र जोशी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी के पास जितनी विषय विविधता थी वो किसी भी लेखक के पास नही थी. उन्होने देश प्रेम की कहानी लिखी पति-पत्नी की कहानी लिखा ब्राम्हणों ठाकुरों पर लिखा. उन्होने उस दौर के सामंति व्यवस्था पर भी रचनाएं लिखी. उस दौर में ऐसा करने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती थी. 1936 से लेकर आज तक कोई ऐसा लेखक नही हुआ जिसके पास विषय की इतनी विविधता थी. वे केवल यर्थाथ के लेखक नही बल्कि साहस के भी लेखक थे. हम जितने प्रेम से उनको याद कर रहे हैं आने वाली पीढि भी उन्हे ऐसे ही याद करेगी.






